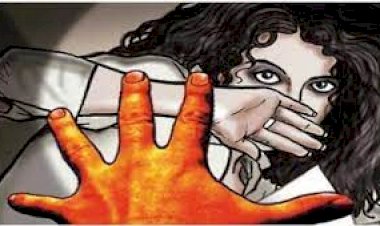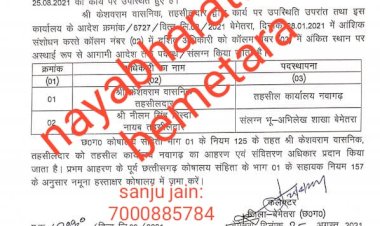पीएम नरेंद्र मोदी देश की सरकारी संस्था को निजीकरण करने वाली संस्था को बेचकर क्या वाकई पीएम मोदी देश हित के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं? हाँ या नहीं.
PM Narendra Modi really doing so much good for




 NBL, 16/01/2023, Lokeshwer Prasad Verma, Raipur CG:Is PM Narendra Modi really doing so much good for the interest of the country by selling the country's government organization to the privatized organization? yes or no..
NBL, 16/01/2023, Lokeshwer Prasad Verma, Raipur CG:Is PM Narendra Modi really doing so much good for the interest of the country by selling the country's government organization to the privatized organization? yes or no..
देश के बहुत से लोगों के दिमाग में ये समझ ही नहीं आ पा रहे हैं, क्या वाकई देश के सरकारी संस्था को पीएम मोदी प्राइवेट कंपनी को बेच कर देश का उन्नति कर रहे हैं या देश के उन्नति में बाधा डाल रहे हैं? हाँ या ना का सही से उत्तर देश के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और इसका मुख्य कारण है, खुद सरकार इस कृत्य का पारदर्शी तरीका से देश के लोगों को पूर्ण रूप से बताने के लिए असमर्थ है, और इन्ही भ्रम को सरकार को हटानी चाहिए, क्योकि सरकारी संस्था का प्राइवेटी करण होना वाकई देश के लोगों के लिए संदेह का मुख्य वजह बन गया है, क्या वाकई पीएम मोदी देश के लोगों को गुमराह मे डाल रहे हैं अपने पूर्ण बहुमत की सरकार के बहुमत का फ़ायदा उठा कर कुछ भी देश में उलट फेर तो नहीं कर रहे हैं, जो आने वाले समय काल में कही देश घोर संकट या देश की आर्थिक स्थिति कमजोर तो नहीं हो जायेगी देश के बारे में यह सब सोचना लोकतंत्र का मूलअधिकार है।
आज कल आपको सोशल मिडिया के प्लेटफार्म में कई बड़े पैमाने पर देश के राजनीतिक नेता व देश के ही आम जनता को इस सरकारी संस्था का प्राइवेट कंपनी के हाथो में जाने का घोर निंदा करते हुए देखने को आपको मिल रहा है, और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के इस प्रकार के डीसीजन से देश के लोगों के दिल दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा है की पीएम मोदी देश को फ़ायदा दिला रहा है या देश के कुछ नामी गिरामी प्राइवेट कंपनी मालिको को फ़ायदा दिला रहे है, बड़े उलझन में पड़े हुए हैं देश के लोग, जो पीएम मोदी का समर्थन करते है वह लोग भी इसका मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, जो अपने विरोधियों को खुलकर जवाब दे सके, इस प्रकार के संधिगता से पीएम मोदी का राजनीतिक ग्राफ व उनके उपर जो विश्वास है देश के लोगों को वह कुछ हद तक गिरने का संभावना बढ़ सकता है।
अगर इस सरकारी संस्था के निजीकरण होने का मुख्य कारण देश के लोगों को बताना या समझाना वर्तमान सरकार का जिम्मेदारी है, तो ही आपके देश हित नीति व नियत देश के लोगों को समझ आयेगी नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी को ये हवा हवाई बातों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है राजनीतिक फ़ायदा मे चुनाव के समय इसलिए समय रहते इस सरकारी संस्था का प्राइवेट कंपनी के हाथो में सौप देने की जानकारी देश के लोकतंत्र को देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र के प्रभाव आपके अनुकूल माहौल बना सकती हैं जो आज आपके साथ है। कल किसी और के पाले में न चला जाएं देश के लोकतंत्र। ये छोटी सी गलती नही है, इसमें बहुत बड़ी गलतीयाँ देख रहे हैं, देश के लोग व देश के नेेता लोग, इसी तरह से आप इनके राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं।
भारत में निजीकरण के लाभ और हानियाँ...
निजीकरण एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के निजी क्षेत्र की कंपनी में परिवर्तन को लागू करने वाला शब्द है। इसके अलावा, जब एक निजी कंपनी पर सरकारी नियमों को कम या हटा दिया जाता है, तो कहा जाता है कि कंपनी "विनियमन" से गुजरी है। "विनियमन" शब्द का प्रयोग अक्सर निजीकरण के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। निजीकरण के फायदे और नुकसान।
दूसरे शब्दों में, निजीकरण का अर्थ है कि किसी विशेष सेवा पर सरकार का नियंत्रण निजी हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया है। निजीकरण के अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों पर फायदे और नुकसान थे। हम "निजीकरण" को उपयुक्त उदाहरणों और इसके गुण-दोषों के साथ समझेंगे।
निजीकरण के उदाहरण. ..
1. स्वास्थ्य सेवा में निजीकरण..
रखो, स्वास्थ्य सेवा में निजीकरण का अर्थ सरकार की स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और सेवाओं में निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की भागीदारी है। इसका मतलब निजी संस्थाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के स्वामित्व का पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण हो सकता है। एक सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है यदि उसे स्वतंत्र रूप से सेवाओं का प्रबंधन या प्रदान करने में कठिनाई होती है - एक बेहतरीन उदाहरण। आइए हम ग्रेट ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निजीकरण के बारे में बात करें। एनएचएस के निजीकरण का मतलब है, जहां सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में बुजुर्गों को भरण-पोषण की नीति अपनाने के बाद राज्य के बजट पर, जब सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, तब स्वास्थ्य उद्योग तेजी से बढ़ रहा है।
2. शिक्षा में निजीकरण
शिक्षा में निजीकरण इसके फायदे, नुकसान और सामाजिक परिणामों पर बहस का एक गर्म विषय रहा है। फिर भी, दुनिया भर में कई सरकारों ने समय-समय पर शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। शिक्षा क्षेत्र की लगातार बढ़ती आवश्यकता और सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता अंततः अकेले सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित करना अधिक कठिन होता जा रहा है; यहां तक कि करदाता के पैसे के माध्यम से शिक्षा के खर्च को वित्तपोषित करना भी अब संभव नहीं है।
3. कल्याण में निजीकरण...
कल्याण में निजीकरण निजी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के पूर्ण या आंशिक प्रबंधन को संदर्भित करता है। इसमें जल आपूर्ति, कौशल और नौकरी प्रशिक्षण, नौकरी के स्थान आदि शामिल हैं। कुछ देशों में, आश्रय गृह और सामुदायिक लंच केंद्र भी निजी खिलाड़ियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। भारत सहित कई देशों ने मुख्य रूप से अपने अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का निजीकरण कर दिया है। हालांकि, सार्वजनिक कल्याण के निजीकरण को सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा यह केवल सरकार को अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से मुक्त करने का एक तरीका बनकर रह जाएगा।
4. बुनियादी ढांचे का निजीकरण...
इंफ्रास्ट्रक्चर के निजीकरण का मतलब राजस्व संग्रह और रखरखाव के लिए निजी संस्थाओं को सड़कों, पुलों और सुरंगों को पट्टे पर देना है। यूरोपीय देशों में इस तरह के सौदे आम रहे हैं, लेकिन आज यह वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ऐसे अनुबंधों के नियम और शर्तें लचीली हैं। एक ठेकेदार जिसने एक विशेष सड़क का निर्माण किया है, को अनुबंध समझौते में परस्पर सहमति के अनुसार पट्टे की समय अवधि के लिए टोल एकत्र करके कंपनी के बिल की एक विशेष राशि वसूलने की अनुमति है।
निजीकरण के कारण...
निजीकरण के कई कारण हैं, जैसा कि सरकारों द्वारा कल्पना की गई है। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से कुछ लागत में कमी, जोखिम हस्तांतरण और राजस्व का अच्छा स्रोत हैं। कई अन्य कारण, जैसे सरकारी एजेंसियों की अक्षमता, और सेवा स्तर में सुधार की इच्छा, भी निजीकरण के वैध कारण हो सकते हैं। नीचे हम संक्षेप में निजीकरण के कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे।
1. लागत में कमी
लागत में कमी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के मुख्य कारणों में से एक है। निजी खिलाड़ियों ने सरकार की तुलना में कम लागत पर लक्ष्य हासिल किया। निजी ठेकेदारों के पास कर्मचारी मुआवज़े और लाभों में अधिक लचीलापन होता है, जो किसी परियोजना की समग्र लागत पर अत्यधिक प्रभाव डालता है।
2.जोखिम का हस्तांतरण...
जोखिम हस्तांतरण एक और कारण है कि क्यों सरकारें कई क्षेत्रों के निजीकरण को प्राथमिकता देती हैं। निजी खिलाड़ियों को एक परियोजना सौंपकर, सरकार एक निश्चित राशि के लिए निजी खिलाड़ी को जिम्मेदारी और जोखिम हस्तांतरित करती है। अब निजी कंपनी के पास प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने, पेनल्टी चुकाने या खुद नुकसान उठाने का जोखिम है।
3. संभावित राजस्व स्रोत...
निजी फर्मों को सड़कों, पुलों और सुरंगों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को पट्टे पर देकर कुछ क्षेत्रों में निजीकरण राजस्व सृजन का एक उपयोगी स्रोत हो सकता है। सौदे से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के लिए सरकार एक अच्छे पट्टे या खरीद समझौते का मसौदा तैयार कर सकती है। इस प्रकार सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए या कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है।
4. सेवा की गुणवत्ता में सुधार...
निजीकरण के मुख्य कारणों में से एक यह है कि सरकार कम लागत पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां/संपर्ककर्ता प्रबंधन में अपनी लचीली नीतियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले कम मुआवजे के कारण लागत को प्रभावित किए बिना सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
5. सुपुर्दगी की समयबद्धता....
निजीकरण के पीछे एक अन्य कारक परियोजना को समय पर पूरा करने की सरकार की इच्छा है। आवश्यक कौशल होने के बावजूद, सरकार कई अन्य बाधाओं के कारण परियोजना को समय पर पूरा करने में असमर्थ हो सकती है। दूसरी ओर, निजी कंपनियों के पास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए 24/7 समर्पित संसाधन हो सकते हैं।
भारत में निजीकरण...
भारत में निजीकरण लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। अतीत में कुछ क्षेत्रों के निजीकरण ने कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों के विरोध को भड़का दिया था; फिर भी, कुछ मामलों में इसे लागू किया गया, जबकि कुछ मामलों में सरकार पीछे हट गई।
भारत में, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, हालांकि वे अत्यधिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं। कई भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों ने कर्मचारियों की अधिकता, अत्यधिक मुआवजा देने वाले कर्मचारियों, परियोजना वितरण में देरी, प्रबंधकीय देरी आदि जैसे कारकों के कारण नुकसान की सूचना दी है।
भारत में निजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे संक्षेप में दिए गए हैं.....
* होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HCL)
प्रारंभ में निजीकरण किया गया, HCL ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया (AI) के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में संचालन किया। सरकार ने एचसीएल संपत्तियों और परिसंपत्तियों के निजीकरण/बिक्री का निर्णय तब लिया जब उसने वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल 15 मिलियन का घाटा दर्ज किया। मुख्य रूप से सरकार और एयर इंडिया द्वारा कुप्रबंधन के कारण HCL लगातार घाटे में थी, जो कि 900 मिलियन से अधिक थी।
* विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल)
1986 में शामिल, विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी संचार सेवाओं को पूरा करना था। 2002 में, भारत सरकार ने टाटा समूह को कंपनी की अधिकतम हिस्सेदारी हस्तांतरित करते हुए, वीएसएनएल के निजीकरण का निर्णय लिया।
निजीकरण के अपने फायदे (फायदे) और नुकसान (नुकसान) हैं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है...
* निजीकरण के लाभ *
1. उत्पादकता में वृद्धि...
एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का निजीकरण दक्षता बढ़ा सकता है क्योंकि निजी उद्यम सरकार की तुलना में अधिक लाभोन्मुखी होते हैं। निजी तौर पर चलाए जाने वाले व्यवसाय के प्रबंधन स्तर के कर्मचारी अधिक लाभ-उन्मुख होते हैं। ब्रिटिश टेलीकॉम (बीटी) और ब्रिटिश एयरवेज निजीकरण के बाद बेहतर दक्षता के दो बेहतरीन उदाहरण हैं।
2. कोई राजनीतिक घुसपैठ नहीं...
सरकार के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निजीकरण करने से सभी राजनीतिक हस्तक्षेप दूर हो जाते हैं, दक्षता में सुधार होता है और घाटे को मुनाफे में बदल दिया जाता है। सरकार द्वारा संचालित उद्यम में प्रबंधक राजनीतिक दबाव में काम करते हैं और इस प्रकार लाभ कमाने के बारे में तर्कसंगत रूप से नहीं सोच सकते। राज्य द्वारा संचालित कंपनियां अक्सर राजनीतिक दबाव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं, अंततः अपने मुनाफे से समझौता करती हैं।
3. दूरदर्शी प्रतिबद्धता...
सरकार द्वारा संचालित कंपनी के अधिकार को निजी हाथों में स्थानांतरित करने का मतलब है कि प्रबंधन को अधिक खुली छूट दी गई है, जो अब दीर्घकालिक लाभ के लिए प्रतिबद्धता बना सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में दूरदर्शिता का अभाव है, जो अल्पकालिक चुनावी लाभ के बारे में अधिक चिंतित है।
4. प्रतिस्पर्धी माहौल....
निजीकरण अधिक से अधिक निजी फर्मों को उद्योग में अपना हाथ आजमाने की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। निजी संस्थाओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से दक्षता लाती है और उन पर गुणवत्ता प्रतिबंध लगाती है। वे नंबर एक होने के लिए अधिक गुणवत्ता और सेवा-उन्मुख हो जाते हैं।
5.राजस्व सृजन...
किसी परियोजना या कल्याणकारी योजना में निवेश के लिए धन की तलाश कर रही सरकार के लिए निजीकरण राजस्व सृजन का एक त्वरित तरीका हो सकता है। सड़कों या पुलों को पट्टे पर देना या उन्हें तुरंत निजी फर्मों को बेचना त्वरित मौद्रिक पुरस्कार लौटाता है; हालाँकि, दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए, यह कुछ मामलों में सरकार के लिए नुकसानदेह है, यदि सभी नहीं।
* निजीकरण के नुकसान....
1. प्राकृतिक एकाधिकार...
कम प्रतिस्पर्धा वाले कुछ क्षेत्रों में निजीकरण से एक निजी फर्म का एकाधिकार हो सकता है। किसी विशेष क्षेत्र पर पूर्ण एकाधिकार होने के कारण, फर्म को अपनी गुणवत्ता से समझौता करने और बड़े मुनाफे का मंथन करने के लिए उच्च मूल्य दर आदि तय करने की खुली छूट मिल जाती है। दूसरी ओर, सरकार द्वारा संचालित एजेंसी ने लाभ से अधिक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी होगी।
2. जनहित में गिरावट...
मुख्य रूप से सार्वजनिक कल्याण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और अन्य में काम करने वाली निजी कंपनियां कल्याण-उन्मुख की तुलना में अधिक लाभ-उन्मुख हैं। यह अत्यधिक करों, उच्च कीमतों और गुणवत्ता और सेवाओं की खराब स्थिति के रूप में आम आदमी को बहुत महंगा पड़ता है।
3.विनियमों का अभाव...
निजीकरण वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय निर्णयों की शक्ति को सरकार से निजी हाथों में ले जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के फैसलों में सरकार की भूमिका सीमित है या नहीं है; न ही सरकार कंपनी के कामकाज या उसकी नीतियों पर ज्यादा नियमन लागू कर सकती है।
4. कम भविष्य का निवेश...
निजी कंपनियां, सरकार के नियमन और नियंत्रण से बाहर, दीर्घकालिक भविष्य की परियोजनाओं से समझौता करते हुए, अल्पकालिक लाभ की तलाश कर सकती हैं। यह कंपनियों को लंबी अवधि के बजाय अल्पकालिक लाभकारी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मजबूर करता है।
5. कंपनियों का विखंडन...
निजीकरण एक विशाल कंपनी को कई अन्य छोटे उद्यमों में तोड़ने का कारण बन सकता है। यह विखंडन अंततः दक्षता को कम करता है और प्रबंधन में जवाबदेही को भी कम करता है। कंपनियां किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल देती हैं और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती हैं।
* निष्कर्ष *
किसी विशेष उद्योग का निजीकरण लंबे समय में फायदेमंद होगा या नहीं यह पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आइए हम परिवहन उद्योग और शिक्षा क्षेत्र की तुलना करें। परिवहन उद्योग में, एकत्रित राजस्व का उपयोग और सुधार के लिए किया जा सकता है। फिर भी, किराया शुल्क को विनियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अधिक शुल्क लेकर जनहित से समझौता कर सकता है। शिक्षा उद्योग में जाने पर, लाभ सृजन का मकसद कम महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए किसी भी निजी फर्म के लिए बिल्कुल नहीं या बहुत कम लाभ के लिए काम करना एक कठिन कार्य होगा। अगर वह ऐसा करती भी है तो इस बात की अधिक संभावना है कि किसी न किसी तरह से जनहित से समझौता किया जाएगा।
देश को झुकने नही दूँगा ना ही देश के उन्नति को रुकने दूँगा।। पीएम नरेंद्र मोदी।।