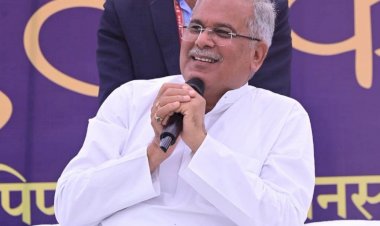युद्ध की बड़ी अजीब विडंबना होती है। पहले तो कोई इसे चाहता नहीं है, लेकिन छिड़ जाए तो कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। रूस-यूक्रेन में छिड़ी लड़ाई को भी क्या किसी दूसरे चश्मे से देखा जा सकता है?




 NBL,. 05/03/2022, Lokeshwer Prasad Verma,....महीनों तक युद्ध की आशंका से सहमी दुनिया को रूसी राष्ट्रपति पुतिन यही दिलासा देते रहे कि उनका यूक्रेन से युद्ध का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ना-ना करते भी वे यूक्रेन से वॉर कर ही बैठे,पढ़े विस्तार से...।
NBL,. 05/03/2022, Lokeshwer Prasad Verma,....महीनों तक युद्ध की आशंका से सहमी दुनिया को रूसी राष्ट्रपति पुतिन यही दिलासा देते रहे कि उनका यूक्रेन से युद्ध का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ना-ना करते भी वे यूक्रेन से वॉर कर ही बैठे,पढ़े विस्तार से...।
हालांकि पुतिन अभी भी इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं, बार-बार वो यही दोहरा रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जा उनका लक्ष्य नहीं है, वो तो बस भटके हुए पड़ोसी को पश्चिमी चंगुल से निकाल कर सही राह पर लाने का 'जतन' कर रहे हैं।
यूक्रेन पर काबू पाने की रूस की कोशिशों के लिए अब शायद 'जतन' शब्द ही उपयुक्त होगा क्योंकि जो काम रूस के लिए एक-दो दिन का लग रहा था, अब वही हफ्तों में भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस लिहाज से यूक्रेन का प्रतिरोध चौंकाने वाला है। हालांकि युद्ध के हालात से जो लोग अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, वो लड़ाई के मैदान से आने वाली हर जानकारी को संदेह की नजर से ही देखने को समझदारी कहते हैं। कारण यह है कि हर युद्ध के समानांतर भ्रामक जानकारियों वाला एक प्रोपेगैंडा युद्ध भी चलता है, जिसका लक्ष्य दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना और उसे दुनिया की नजर में खलनायक साबित करना होता है। बेशक, यूक्रेन इस क्षेत्र में पश्चिमी मीडिया की सरपरस्ती में रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन महज इस आधार पर ही रूस किसी संवेदना का अधिकारी भी नहीं हो जाता। दरअसल, पुतिन ने यूक्रेन की प्रतिरोध की मात्रा का गलत अनुमान लगा लिया।
जो सोचा हुआ उसका उल्टा
लगता है पुतिन ने यह मान लिया था कि जैसे ही रूसी सैनिक सीमा पार करेंगे, यूक्रेन आत्मसमर्पण कर देगा और उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। नाटो और अमेरिकी सेना के युद्ध में कूदने से इनकार के बाद लड़ाई में अकेले पड़े जेलेंस्की ने यूक्रेन की राजधानी कीव में जैसे खम ठोक दिया और नाटो से मिले हथियारों को अपनी अवाम में बांट कर हर यूक्रेनी को जैसे सैनिक बना दिया। पश्चिम के तमाम प्रचार के बावजूद इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दस दिन के युद्ध के बाद भी रूस के हाथ खाली ही हैं। न उसका यूक्रेन के आसमान पर कब्जा हो पाया है, न जमीन के किसी टुकड़े पर। अब जमीनी हालत यह है कि यूक्रेनियन हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जबकि रूसियों को वास्तव में जीतना है। रूस की पसोपेश यह है कि यह जानते हुए भी कि यूक्रेन को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, उसे यह युद्ध हाथ बांध कर लड़ना पड़ रहा है। संभवत: इसकी वजह यूक्रेनी नागरिकों को कम-से-कम नुकसान पहुंचाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि इसके कारण लंबे खिंच रहे युद्ध से पुतिन का घमंड और संयम, दोनों टूट रहा है, नहीं तो उन्हें परोक्ष रूप से ही सही, परमाणु हमले की धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती।
वैसे परमाणु हमले की धमकी देने के पीछे यही एक वजह नहीं है। अमेरिका समेत रूस विरोधी मोर्चे की रणनीति भी पुतिन के संयम का इम्तिहान ले रही है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद अब पश्चिमी देशों में पुतिन और उनके समर्थक ओलिगार्क पर पाबंदी लगाने की होड़ दिख रही है। रूस के केंद्रीय बैंक को अमेरिकी डॉलर के लेन-देन से काट दिया है, और प्रमुख रूसी बैंकों को महत्त्वपूर्ण स्विफ्ट के वैिक वित्तीय नेटवर्क से बाहर कर दिया है। सबसे असाधारण बदलाव जर्मनी के रु ख में आया है, जो न केवल यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए राजी हुआ है, बल्कि उसने पश्चिमी यूरोप के लिए अत्यधिक आवश्यक रूसी गैस लाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन को भी रोक दिया है। पुतिन के पिछलग्गू कहलाने वाले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोआन भी पाला बदल कर यूरोपीय संघ के साथ हो गए हैं। उधर, लंदन में महंगी संपत्तियों से धनकुबेर बने ओलिगाकरे से लंबे समय तक आंखें मूंदे रहने के बाद ब्रिटेन ने भी उनके खाते फ्रीज करने शुरू कर दिए हैं। जहां तक आर्थिक प्रतिबंधों की बात है, तो बलशाली देशों ने उन्हें कभी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि समय के साथ वो अप्रभावी भी हो जाते हैं, लेकिन इनका तात्कालिक असर यह हुआ है कि रूसी रूबल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 41 फीसद तक नीचे आ गया जो साल 1998 के बाद रूबल की सबसे बुरी स्थिति है। रूबल के एक्सचेंज रेट की बात करें तो भारत का रु पया भी 1.32 रूसी रूबल के बराबर आ गया यानी एक समय के कारोबार में भारतीय रु पया भी रूबल से मजबूत हालत में नजर आने लगा। रूस निश्चित रूप से अपने खिलाफ हो रही इस गोलबंदी से जल्द-से-जल्द उबरना चाहेगा। लेकिन इसके लिए उसका रोडमैप क्या हो सकता है? रूस को सबसे पहले तो यूक्रेन पर अपना नियंतण्रस्थापित करना होगा। सारा झगड़ा इसी बात का है कि पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो पाए क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यूक्रेन क्रीमिया पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर सकता है। इसके लिए पुतिन यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से यह मांग करते रहेंगे कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन वहां अपनी पसंद का शासन स्थापित करें जो रूसी संप्रभुता के उनके विचारों को आगे बढ़ाए। पुतिन यूक्रेन को व्यापक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) में भी शामिल कर सकते हैं, जो पूर्व सोवियत संघ देशों के लिए बनाया गया था और रूस द्वारा नियंत्रित होता है। फिलहाल तो यह केवल पुतिन का सपना ही दिखता है क्योंकि सच तो यह तभी होगा जब रूसी सेना यूक्रेन पर फतह हासिल करेगी।
पश्चिम के सामने भी होंगे कई सवाल...
हो सकता है कि रूस आने वाले दिनों में इस सपने को साकार भी कर ले, लेकिन इसके साथ ही रूस समेत पश्चिम को भी कई ऐसे सवालों का सामना करना होगा जिसके जवाब शायद दशकों तक ना मिलें? पहला सवाल तो यही होगा कि क्या इस जंग को रोका जा सकता था? शायद हां। अगर अमेरिका, जर्मनी और दूसरे पश्चिमी देश साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के समय हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठे रहते तो शायद आज का मंजर कुछ और होता। क्रीमिया की सफलता के खुमार ने ही पुतिन को पहले डोनबास और अब समूचे यूक्रेन में तांडव मचाने की प्रेरणा दी। दूसरा महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस जंग ने यूरोप को बैठे-बिठाए शरणार्थी संकट में झोंक दिया है? हालात तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का अनुमान है कि 40 लाख लोग यूक्रेन छोड़ कर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और रूस का रु ख कर सकते हैं। यह साल 2011 में सीरिया के गृहयुद्ध वाली स्थिति है, जब 56 लाख लोगों ने पड़ोसी मुल्कों में पलायन किया था। महत्त्व का तीसरा सवाल है कि क्या अब मान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है? हो सकता है यह मान लेना अभी भी जल्दीबाजी हो, लेकिन पिछले अनुभव तो यही बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र केवल हेल्पलेस ही नहीं, होपलेस भी दिखने लगा है। बार-बार रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाकर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि रूस के पास पूरी दुनिया को चिढ़ाने वाला संयुक्त राष्ट्र का ही दिया हुआ वीटो पावर जो है। शायद ऐसे ही विशेषाधिकारों से पोषित होती मजबूत देशों की हिमाकत उसे चौथे सवाल को जन्म देती है कि आखिर, दो बड़े और कई छोटे-छोटे युद्ध के बावजूद मानवता को खतरे में डालने की प्रवृत्ति का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है?
भारत का रुख तटस्थ..
इस युद्ध पर भारत का रु ख फिलहाल तटस्थ बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाला यूएनएससी प्रस्ताव, मानवाधिकारों पर यूएनएचसीआर प्रस्ताव और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाने के प्रस्ताव पर भारत वोटिंग से दूर रहा है। भारत के रुख की सार्थकता पर दो धारणाओं में संघर्ष दिख रहा है। पहली धारणा तो रूस पर हमारी निर्भरता है। पुरानी दोस्ती और हथियारों की आपूर्ति के साथ ही कश्मीर मामले में पाकिस्तान के साथ विवाद में भारत रूस के सहयोग और सुरक्षा परिषद में वीटो के लिए निर्भर रहा है। रूस से दोस्ती चीन को साधने में भी काम आ सकती है, और विरोध करना उसे पूरी तरह चीन के खेमे में जाने को मजबूर कर सकता है। इसके विपरीत दूसरी धारणा यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो भी यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। युद्ध से पुतिन कमजोर होते हैं, तो वो चीन की वैिक पहुंच को बाधित करेगा। रूस के संबंधों के कारण ही चीन मध्य-पूर्व में पैठ बना पाया। मध्य-एशियाई गणराज्यों में चीन के आर्थिक और सैन्य दबदबे की वजह भी रूस ही है। चीन के महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की यूरोप तक पहुंच रूस के अलगाव से धराशायी भी हो सकती है।
इससे समझ आता है कि तटस्थ रहने के बावजूद एशिया से लेकर यूरोप तक के तमाम देशों का किस तरह इस युद्ध से किसी-न-किसी रूप में वास्ता जुड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि युद्ध का अंजाम आखिर क्या होगा? अगर यूक्रेन की सीधी मदद नहीं करने की नाटो और पश्चिम की रणनीति में कोई खास बदलाव नहीं आता है, तो यह तय है कि देर-सबेर रूस इस युद्ध को जीत ही लेगा। लेकिन इस जीत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन की सड़कों और गलियों में बह रहे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों के खून ने वैिक ही नहीं, घरेलू मोर्चे पर भी रूस पर मानवता के दुश्मन का ठप्पा लगा दिया है। सोवियत साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए एक रक्तहीन क्रांति ही शायद पुतिन के मकसद को वो पवित्रता दे सकती थी, जो उन्हें दुनिया में नायक की तरह स्थापित करती। फिर अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका का हश्र बताता है कि जंग से जीते गए देशों पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना आसान नहीं होता। वैसे लंबे समय से हम यह भी सुनते आए हैं कि जो जीता, वही सकिंदर। तो क्या आने वाले दिनों में जीत कर भी बाजी हारने वाले को अब रूस कहा जाएगा?