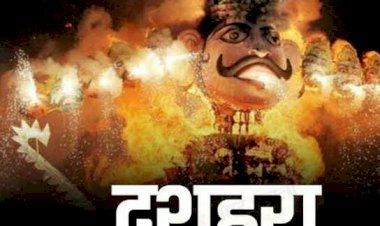सुख कितने प्रकार के होते हैं ? सुख तीन प्रकार के होते हैं – सात्त्विक,राजसिक एवं तामसिक..
How many types of happiness are there?




 NBL,30/12/2022, Lokeshwer Prasad Verma, Raipur CG: How many types of happiness are there? Happiness is of three types – sattvic, rajasic and tamasic.
NBL,30/12/2022, Lokeshwer Prasad Verma, Raipur CG: How many types of happiness are there? Happiness is of three types – sattvic, rajasic and tamasic.
सात्त्विक
अपने सुख-दुःख का विचार न कर, दूसरों को सुख देना । दूसरों को सुख देने से अपना सुख नहीं घटता, यही खरा १०० प्रतिशत सुख है । यह मन का सुख होता है।
राजसिक
दूसरों को दुःख न देकर केवल अपने लिए सुख की प्राप्ति करना । ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय द्वारा मिलनेवाले सुख को राजसी सुख कहते हैं; उदाहरणार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ खाना । यहां तत्काल सुख अथवा तृप्ति मिलती है; परंतु अंततः नीचे दिए कारणों से उसका रूपांतर दुःख में ही हो जाता है।
१. बहुत अधिक सुख का भी उपभोग नहीं किया जा सकता; उदाहरण के लिए, मीठे पदार्थ अधिक खाने से अपच हो सकता है।
२. इच्छा होने पर उसी क्षण इच्छित पदार्थ उपलब्ध नहीं हो सकता; उदाहरण के लिए, मिठाई की दुकान बंद होना अथवा वह मिठाई उस दुकान पर उपलब्ध न होना।
३. कभी-कभी सुख आवश्यकता में रूपांतरित हो जाता है; उदाहरण के लिए, गाडी से आना-जाना अच्छा लगने लगे, तो गाडी पर निर्भरता हो जाती है । ऐसे में, किसी दिन गाडी उपलब्ध न हो तो दुःख होता है।
तामसिक
दूसरों को दुःख देने में एवं जीवन के कष्टों से दूर भागने में ही व्याqक्त को सुख मिलता है; उदा. मद्यपान करना, मादक पदार्थों का सेवन करना।
बौद्धिक सुख सात्त्विक होता है, मानसिक सुख राजसिक एवं स्थूलदेह का सुख तामसिक स्वरूप का होता है।
सुखप्राप्ति एवं दुःखनिवृत्ति के प्रयत्न....
सुखप्राप्ति के प्रयत्न
पाठशाला, महाविद्यालय आदि में इतिहास, भूगोल, गणितादि विषय पढाते हैं; परंतु आनंद कैसे पा सकते हैं, यह नहीं सिखाया जाता । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पंचज्ञानेंद्रिय, मन व / या बुद्धि से अधिकाधिक सुखप्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है । विषय सुख भोगने के लिए मनुष्य विवाह करता है एवं तदुपरांत दुःख भुलाने के लिए विषयसुख भोगता है । विषय सुख भोगने से दुःख को अल्पकाल के लिए ही भुलाया जा सकता है; परंतु उसे दूर नहीं किया जा सकता।
दुःखनिवृत्ति के प्रयत्न
यन्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो वा दुःखमेव च ।
आयासो वा यतो मूलमेकाङ्गमपि तत्त्यजेत् ।।
* महाभारत, सभापर्व, अध्याय १७४, श्लोक ४३
अर्थ : जिसके कारण शोक, यातना, दुःख अथवा कष्ट होते हैं, वह कारण भले ही हमारे शरीर का एक अवयव हो, तब भी उसका त्याग करना चाहिए।
सुखप्राप्ति के प्रयत्न की अपेक्षा, मानव के अधिकांश प्रयत्न दुःख घटाने के लिए होते हैं । स्वास्थ्य ठीक न हो तो डॉक्टर के पास जाना, आकाशवाणी संच (रेडियो), वाहन आदि बिगड जाए तो ठीक करवाना, इस प्रकार मनुष्य उन परिाqस्थतियों में होनेवाले दुःख को घटाने का प्रयत्न करता है । स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना, वाहन न बिगडे इसलिए समय-समय पर उसकी स्वच्छता एवं मरम्मत करवाना, ऐसे प्रयत्न बहुत ही अल्प लोग नियमित रूप से करते हैं । दुःख दूर करने के प्रयत्न भी सदा सफल नहीं होते । असामान्य रोग, बुढापा एवं मृत्यु, ये बातें ऐसी हैं कि सामान्य मनुष्य उनसे होनेवाले दुःख को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता।
संक्षेप में, आनंदप्राप्ति कैसे करनी है, यह ज्ञात न होने के कारण अल्पकाल टिकनेवाले छोटे सुखों की प्राप्ति एवं दुःखों को दूर करने के प्रयत्न में ही अधिकांश लोगों का जीवन बीत जाता है।
१. प्रत्येक सुख में दुःख अंतर्भूत होता है
जैसे रुिचकर पदार्थ खाना, गाने सुनना, सिनेमा देखना आदि बातें आरंभ में सुख देती हैं; परंतु वही बातें पुनः-पुनः करने से उनसे मिलनेवाला सुख घटता जाता है एवं अंत में यही बातें दुःख देने लगती हैं।
जब कोई मनुष्य पदार्थ, उदाहरण के लिए आईस्क्रीम खाने लगता है, तब पहली २-४ प्लेटें वह चाव से खा लेता है । अगली २-४ प्लेटें वह अल्प चाव से खाएगा एवं उसके उपरांत आईस्क्रीम दिए जाने पर वह मना कर देगा । बलपूर्वक खिलाने पर उसे उससे दुःख भी होगा । यही स्थिति कोई भी एक गाना बार-बार सुनने से अथवा सिनेमा बार-बार देखने से होती है । एक मीठा पदार्थ (उदा. लड्डू) खाने से सुख मिलता है; परंतु वैसे २० पदार्थ खाने से पेट में वेदना होने लगती है अथवा अतिसार (जुलाब) हो जाता है । इसका अर्थ है कि प्रत्येक मीठा पदार्थ खाने में १/२० भाग दुःख छिपा होता है । इसलिए अध्यात्मरामायण में कहा है कि प्रत्येक सुख में दुःख छिपा होता है।
२. सूक्ष्मदेह (वासनादेह, मनोदेह) से मिलनेवाला सुख
मन से मिलनेवाला सुख; उदा. किसी से प्रेम करने पर । यह सुख पंचज्ञानेंद्रियों द्वारा मिलने वाले सुख की अपेक्षा उच्च श्रेणी का एवं अधिक मात्रा में होता है । वह अधिक समय टिकता भी है । आगे प्रेमपूर्ति हो जाए, तो उससे मिलनेवाला सुख अल्प हो जाता है।
३. कारणदेह से (बुद्धि से) मिलनेवाला सुख
किसी विषय का अभ्यास करना, अभ्यास कर उसे समझना, गणित के किसी कठिन प्रश्न का हल होना, अन्वेषण द्वारा कुछ नया शोध लगाना आदि से मिलनेवाले सुख मानसिक सुख की अपेक्षा उच्च श्रेणी का एवं अधिक मात्रा में होता है; परंतु यह भी अल्प समय ही टिकता है।
४. इंद्रियों द्वारा मिलनेवाले सुख की मात्रा
इस सारणी से यह स्पष्ट होगा कि किसी की कोई ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रिय कार्यरत न हो, तब भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरणार्थ कोई पूर्णतः बहरा हो अथवा दोनों पैरों से लंगडा हो, तो उसे अन्यों की तुलना में केवल २ प्रतिशत ही सुख अल्प मिलेगा । ऐसा होते हुए भी अधिकांश लोगों में उनके अपंगता के कारण हीन भावना निर्माण होती है और वे अधिक दुःखी हो जाते हैं।