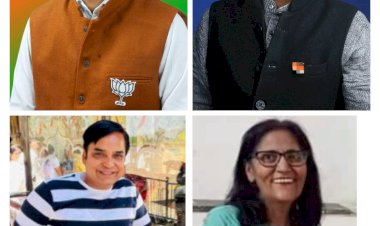किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा-बुरा या सही-गलत की परख की जाती है.
Values play an important role in the life of any human.




 NBL, 15/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Values play an important role in the life of any human being because on the basis of these, good or bad or right and wrong are judged.
NBL, 15/05/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. Values play an important role in the life of any human being because on the basis of these, good or bad or right and wrong are judged.
समाज में बढ़ रही हिंसक मानसिकता ने इस नैतिकता को ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है जहां व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, चारित्रिक व नैतिक पतन की ओर बढ़ता जा रहा है, पढ़े विस्तार से...
इस डिजिटल युग में इन नैतिक मूल्यों का ह्रास भी डिजिटल होता जा रहा है और साइबर अपराध इसका सर्वोचित उदाहरण हो सकता है. किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा-बुरा या सही-गलत की परख की जाती है। इंसान के जीवन की सबसे पहली पाठशाला उसका अपना परिवार ही होता है और परिवार समाज का एक अंग है। उसके बाद उसका विद्यालय, जहां से उसे शिक्षा हासिल होती है। परिवार, समाज और विद्यालय के अनुरूप ही एक व्यक्ति में सामाजिक गुणों और मानव मूल्यों का विकास होता है।
किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा-बुरा या सही-गलत की परख की जाती है। इंसान के जीवन की सबसे पहली पाठशाला उसका अपना परिवार ही होता है और परिवार समाज का एक अंग है। उसके बाद उसका विद्यालय, जहां से उसे शिक्षा हासिल होती है। परिवार, समाज और विद्यालय के अनुरूप ही एक व्यक्ति में सामाजिक गुणों और मानव मूल्यों का विकास होता है।
प्राचीन काल के भारत में पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी जरूरी होती थी। लेकिन वक्त के साथ यह कम होता चला गया और आज वैश्वीकरण के इस युग में मूल्य आधारित शिक्षा की भागीदारी लगातार घटती जा रही है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, हिंसा, असहिष्णुता और चोरी-डकैती आदि की बढ़ती प्रवृत्ति समाज में मूल्यों के विघटन के ही उदाहरण हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15 किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव की मुखालफत करता है। लेकिन सच यह है कि संविधान लागू होने के पैंसठ साल बाद भी हमारे विद्यालयों में जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। विभिन्न विद्यालयों में अपने शिक्षण अनुभवों के दौरान मैंने देखा कि विद्यालय में पानी भरने के अलावा सफाई का काम लड़कियों से ही कराया जाता है।
अध्यापक पीने के लिए पानी कुछ खास जाति के बच्चों को छोड़ कर दूसरी जातियों के बच्चों से ही मंगवाते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने में आए कि बच्चे मिड-डे-मील अपनी-अपनी जाति के समूह में ही बैठ कर खा रहे थे। स्कूल में कबड्डी जैसे खेल सिर्फ लड़के खेलते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे आसपास के स्कूलों में देखने को मिल जाएंगे।
हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी ने वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक मूल्यों की सूची तैयार की है। इसका बदलाव हम प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में भी देख सकते हैं। कुछ साल पहले तक पाठ्यपुस्तकों में भी भेदभाव करने वाले चित्र नजर आते थे, मसलन, झाड़ू लगाती हुई लड़की, खाना बनाती औरतें, हल चलाते हुए किसान और उपदेश देते गुरु आदि। लेकिन पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के बाद इन चित्रों में गुणात्मक बदलाव देखने को मिलता है। मसलन, सफाई करते हुए लड़के और खेलती हुई लड़कियां आदि।
पाठ्य-पुस्तकों में जाति, धर्म और लिंग आधारित चित्रों में जो रूढ़िबद्ध जड़ता थी, उससे आगे बढ़ कर अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। यह बदलाव केवल चित्र के स्तर पर नहीं, बल्कि विषय-वस्तु और निर्देशों के स्तर पर भी देखा जा सकता है।
लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन मूल्यों की बात पाठ्य-पुस्तक करती है, उनका उपयोग शिक्षक विद्यालय में कैसे कर रहा है! यह एक अजीब विडंबना है कि पाठ्यपुस्तकों से शिक्षाविदों ने सामाजिक और मानवीय भेदभाव को अभिव्यक्त करने वाले चित्रों को तो बदल दिया, मगर विद्यालयी वातावरण में वह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है।
आमतौर पर शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाना और नैतिक सीख देना ही काफी समझते हैं और विद्यार्थी के व्यवहार में मूल्यगत बदलाव पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि जिस जाति या समाज से शिक्षक संबंध रखता है, उसके मुताबिक उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। उन अतार्किक जड़बद्ध सामाजिक-धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से शिक्षक तर्कशील होकर नहीं सोच पाता है, क्योंकि उस पर जाति, धर्म और समाज विशेष की पहले से बनी धारणाएं हावी रहती हैं। उन्हीं रूढ़िबद्ध मान्यताओं के अनुसार वह चलना चाहता है। लेकिन जब तक शिक्षक अपने आपको तर्क की कसौटी पर रख कर नहीं सोचेगा, तब तक वह न तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है और न ही विद्यार्थियों में मूल्यों के प्रति आस्था विकसित कर सकता है।
एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि वह पाठ्य-पुस्तकों में दिए गए ‘मूल्यों’ का महत्त्व समझे, उन्हें अपने जीवन व्यवहार का हिस्सा बनाए, फिर बच्चों के दैनिक व्यवहार में लाने का प्रयास करे। स्कूलों से समाज की अपेक्षा होती है कि वह तर्कशील मनुष्य प्रदान करे। इसलिए स्कूलों में ही जरूरी मानव मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई तो कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने से हम चूक जाएंगे। लिहाजा, आवश्यक है कि पाठ्य-पुस्तकों में उल्लिखित मूल्यों के प्रति शिक्षक समाज चिंतनशील हो, उन्हें बच्चों के दैनिक जीवन में लेकर आए।