आत्मा और परमात्मा का मिलन ब्रह्मविद्या बौद्धिक जिज्ञासा या युक्तिसंगत खोजबीन है। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है?..
union of soul and divine Theosophy is intellectual curiosity or rational investigation. We want to know what the world is?
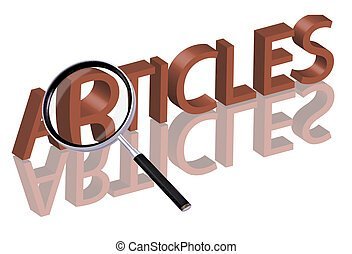



 NBL,. 21/03/0/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. Raipur cg: मेरे सज्जन प्रिय पाठकों के लिए एक सुंदर सा लेख..पढ़े विस्तार से...।
NBL,. 21/03/0/2022, Lokeshwer Prasad Verma,.. Raipur cg: मेरे सज्जन प्रिय पाठकों के लिए एक सुंदर सा लेख..पढ़े विस्तार से...।
आत्मा और परमात्मा का मिलन 'कृष्णार्जुन संवाद' है। यही अंत है, यही लक्ष्य है यही पूर्णता है। तुम्हें उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संपृक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं।
आपको उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संपृक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं। आज विश्व धर्म के प्रति अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है। विज्ञान और औद्योगिकी की जबर्दस्त और चमत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन एक गहरे शून्य से भर गया है। वह नहीं जानता कि इस शून्य को कैसे भरा जाए।
चूँकि आज लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, इसलिए वे हर चीज की छानबीन और पूछताछ करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखनी होंगी जो उन्हें बौद्धिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से आश्वस्त कर सकें। हमें भी किसी ऐसे धर्म को उनके सामने नहीं रखना है जो युक्तिमूलक न हो। हर कोई हमसे पूछता है, क्या यह युक्तिसंगत धर्म है? हर कोई धर्म के बारे में जिज्ञासा रखता है और यही वास्तव में हमारा अभीष्ट भी है। क्या धर्म का लक्ष्य तर्क और चेतना के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है?
जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, हमने इन सभी बातों पर जोर दिया है। भगवद्गीता के अंत में दी गई पुष्पिका में कहा गया है, 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे।' ब्रह्मविद्या बौद्धिक जिज्ञासा या युक्तिसंगत खोजबीन है। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया क्या है? यही ब्रह्मविद्या है।
व्यावहारिक अनुशासन को, जो बौद्धिक विचार को जीवन के विश्वास में परिणत कर देता है, 'योगशास्त्र' कहा गया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन 'कृष्णार्जुन संवाद' है। यही अंत है, यही लक्ष्य है यही पूर्णता है। तुम्हें उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संपृक्त है और जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं।
क्या कोई ऐसी व्यापक और संपृक्त चीज है जिसमें इन सभी क्रियाओं का संपृक्त रूप में समावेश हो जाता है? यह प्रश्न है। वह उत्तर देता है, 'इसे तुम्हें तप से सीखना होगा।' फिर उत्तर देता है, 'तपोब्रह्म' अर्थात् 'तप' करने से। इस जिज्ञासा का मूल कारण है तुममें अंतर्निहित दिव्यशक्ति की हलचल। चूँकि तुममें दिव्यशक्ति मौजूद है, इसलिए तुम स्पष्टीकरण माँगते हो। अगर वह शक्ति मौजूद न होती तो तुम स्पष्टीकरण न माँगते। इसीलिए वह कहता है, 'तपोब्रह्म' और ब्रह्म विजिज्ञासस्व अर्थात् तप से ही तुम जान पाओगे कि वह क्या है।
ज्ञानि के अनुसार तप का अर्थ है आलोचना अर्थात् किसी वस्तु को पहली बार देखने से संतुष्ट न होने पर पुनर्विचार करना। यही तपस्या है। अगर तुम प्रयास करो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यह विश्व मात्र एक आकस्मिक घटना नहीं है और न ही इसे किसी प्रकार की सनक माना जा सकता है। तुम्हारे सामने एक के बाद एक मूल्यों का निरंतर उद्घाटन होता जाएगा। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन और मन से बुद्धि का एक निश्चित क्रम है। इसके बाद जाकर तुम्हें आत्मशांति मिलती है, जिसे परम आनंद कहा गया है।
आध्यात्मिक मुक्ति इस दुनिया का मूल है और इसी मुक्ति से बुद्धि, मन, जीवन और पदार्थ प्रकट होते हैं। कितना अच्छा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण अच्छा ही होता है क्योंकि इससे हमें बात समझ में आती है। यह हठधर्मिता नहीं है। किसी महात्मा या अन्य व्यक्ति के कहने से हमने इसे नहीं माना है। यह दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है और इसी की सहायता से हम यह मानने की कोशिश करते हैं कि यह दुनिया आखिर है क्या। 'ब्रह्मविद्या' के बाद आता है 'योगाशास्त्र'। सिर्फ 'ब्रह्मविद्या' से बात नहीं बनेगी। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही आपको आध्यात्मिक जीव नहीं बना देगा। आपके संदेहों के निवारण के लिए योगशास्त्र बहुत जरूरी है।
विज्ञान विश्व की बाहरी सतह और उसकी विविधता और बहुलता पर दृष्टि डालता है लेकिन उसके केंद्रबिंदु की अनुभूति तो केवल एकांतिक ध्यान से ही हो सकती है। यही वह केंद्रबिंदु है जिससे ये सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसे बौद्धिक भाषणों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को अलग करना होगा अर्थात् संसार की घटनाओं से असंपृक्त होकर ही आप इस केंद्रबिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ईश्वर की रचना को समझ सकते हैं।
 मनुष्य का जीव एकाचित स्थान पर ठहर नही सकते क्योकी उनके आत्मा संसार के अन्य जरूरतो के लिए घेरे हुए हैं, चक्रव्यहूह की तरह' इसलिए तो ईश्वर का स्वरूप को नही जान पाते जबकि उनकी सुख उनके पास है जिसका नाम है जीवआत्मा जिसको सही सुख दे सकते हैं वह है आत्म कल्याण जो अपने आप से संतुष्ट होने पर मिलती है, इससे बड़ा कोई ईश्वर की शक्ति इस संसार में नही है। इसी का नाम जीव आत्मा हम जीव व परमात्मा वह सुख जिसका नाम है परमआनंद इस आत्म स्वरूप के साथ आपके जीव जुड़ गया मतलब आप इस संसार के सबसे बड़े सुखी इंसान।
मनुष्य का जीव एकाचित स्थान पर ठहर नही सकते क्योकी उनके आत्मा संसार के अन्य जरूरतो के लिए घेरे हुए हैं, चक्रव्यहूह की तरह' इसलिए तो ईश्वर का स्वरूप को नही जान पाते जबकि उनकी सुख उनके पास है जिसका नाम है जीवआत्मा जिसको सही सुख दे सकते हैं वह है आत्म कल्याण जो अपने आप से संतुष्ट होने पर मिलती है, इससे बड़ा कोई ईश्वर की शक्ति इस संसार में नही है। इसी का नाम जीव आत्मा हम जीव व परमात्मा वह सुख जिसका नाम है परमआनंद इस आत्म स्वरूप के साथ आपके जीव जुड़ गया मतलब आप इस संसार के सबसे बड़े सुखी इंसान।

































